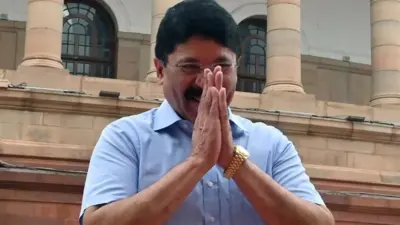इराक़ संकट के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
इराक़ में गहराते संकट ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चुनौती पेश की है.
बीबीसी ने कोशिश की इस संकट से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कुछ विशेषज्ञों के साथ:
शिया सुन्नी टकराव से बढ़ा संकट
डॉक्टर काओ चुकुई,
अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, चीन की केंद्रीय समिति का पार्टी स्कूल
मौजूदा संकट की दो वजह हैं. पहली, सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाएं मज़बूत हुई हैं. जो संघर्ष एक सरकार और उदारवादी विपक्ष के बीच था वो संघर्ष अब त्रिकोणीय हो गया जिसमें सरकार, विपक्ष और आईएसआईएस जैसे चरमपंथी संगठन शामिल हैं.
सीरियाई सरकार की स्थिति मज़बूत होने के कारण उसने आईएसआईएस जैसे संगठनों के लिए हालात मुश्किल कर दिए और वे उत्तरी इराक़ की तरफ़ जाने को मजबूर हुए हैं.
दूसरी वजह, इराक़ी प्रधानमंत्री नूर अल मलिकी के नेतृत्व में शियाओं ने राजनीतिक रूप से सुन्नियों का शोषण किया है जिससे उनके बीच संकट और गहरा गया. इससे आईएसआईएस की गतिविधियों को उपजाऊ जमीन मिली.
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में इराक़ का दौरा किया और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया. मलिकी चुनाव के जरिए सत्ता में आए हैं, इसीलिए चीनी सरकार को उम्मीद है कि वो स्थिरता क़ायम करने के लिए क़दम उठा सकते हैं. चीन के हस्तक्षेप की अपीलें हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन ऐसा कदम उठाएगा.
चीन की तीन सबसे बड़ी कंपनियों ने इराक़ में निवेश किया है. वो स्थिति पर नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं. अभी उन्होंने अपने कर्मचारियों को वहां से नहीं हटाया है.
निश्चित तौर पर चीनी सरकार वहां की स्थिति को लेकर चिंतित है और इसका असर पहले ही तेल के अस्थिर बाज़ार पर पड़ने लगा है. इराक़ में स्थिरता बहाल करना न सिर्फ चीन बल्कि सभी इराक़ियों के भी हित में है.
आईएसआईएस: मध्य पूर्व के लिए नई चुनौती
वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख़बरें जो दिनभर सुर्खियां बनीं.
दिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर
समाप्त
एरियल गोंज़ालेज़ लेवागी
मध्य पूर्व विशेषज्ञ और अर्जेंटीना अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के निदेशक
मोसूल और अन्य अहम सुन्नी शहरों पर आईएसआईएस का नियंत्रण होना इराक़ और वर्तमान मध्य पूर्व के बुनियादी आधारों को लिए एक चुनौती है.
1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए गोपनीय साइक्स-पिकोट समझौते के तहत ऑटोमन साम्राज्य को फ्रांस, ब्रिटेन और रूसी प्रभाव वाले इलाकों में बांट दिया गया.
आज के मध्य पूर्व की ज़्यादातर सीमाओं का निर्धारण और देशों को क्षेत्रों का वितरण इसी 98 साल पुराने समझौते के आधार पर किया गया. साइक्स-पिकोट मध्य पूर्व वो क्षेत्र है जिसे पश्चिमी कूटनीति के आधार पर तैयार किया गया था.
आईएसआईएस मौजूदा सीमाओं को बदलकर क्षेत्र में एक इस्लामी शासन क़ायम करना चाहता है. इस्लामी चरमपंथियों ने एक नई सुन्नी धुरी तय की है जो सीरिया में एलेप्पो शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित अल-बाब से लेकर इराक़ में मोसूल और फलूजा तक जाती है.
आधुनिक मध्य पूर्व की सीमाओं को नए सिरे से खींचने के लिए इस्लामी कट्टरपंथ को विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लिए आर्थिक मदद कुवैत, क़तर और सऊदी अरब से मिल रही है और बड़ी मात्रा में हथियार विभिन्न स्रोतों से मिल रहे हैं. साथ ही समर्थन स्थानीय क़बीलों और इराक़ में बाथ पार्टी के पूर्व सदस्यों की तरफ से हासिल हो रहा है.
लेकिन इराक़ में मौजूदा स्थिति अमरीका के हस्तक्षेप के बाद और बिगड़ी है. 2003 में इराक़ पर हुए हमले ने शिया और सुन्नी समुदायों के बीच मतभेदों को और उजागर कर दिया.
अमरीकी सैन्य हस्तक्षेप के बाद से कोई भी इराक़ी सरकार देश के सभी हिस्सों पर नियंत्रण नहीं कर पाई है. अब सुरक्षा स्थिति भारी अव्यवस्था का शिकार है और लगभग सभी सुन्नी आईएसआईएस के शासन में रहे हैं जिसका नेतृत्व अबु बकर अल-बग़दादी कर रहे हैं. उन्हें नया ‘जिहादी सितारा’ माना जा रहा है.
आईएसआईएस के सैन्य विस्तार का तीन क्षेत्रीय शक्तियों तुर्की, ईरान और सऊदी अरब पर असर होगा. इन तीनों देशों के बीच क्षेत्र में अपना वर्चस्व क़ायम करने के लिए संघर्ष जारी है.
ईरान एक नए कट्टरपंथी सुन्नी क्षेत्र के निर्माण को लेकर चिंतित है. तुर्की को भी इससे सीधा ख़तरा महसूस हो रहा है. इस पूरे घटनाक्रम का सऊदी अरब को फायदा होगा, जो इराक़ी सरकार के मुकाबले विचारधारा और राजनीति के स्तर पर आईएसआईएस के कहीं ज़्यादा क़रीब है.
मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय शक्तियों और गठबंधनों के पुनर्गठन का नहीं है, इस संकट के कारण तेल के दाम भी बढ़ेंगे. नया मध्य पूर्व अस्तित्व में आ रहा है और ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है.
दो पाटों के बीच इराक़
आमिर ताहेरी
ईरान में जन्मे लेखक और पत्रकार
ये बहस असल में एक राष्ट्र के तौर पर इराक़ के बारे में नहीं है. 2003 के जिस युद्ध में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल किया गया, उसे विदेश नीति का एक मुद्दा नहीं समझा जाता है, बल्कि उसे अमरीका और ब्रिटेन की घरेलू राजनीति के तौर पर देखा जाता है.
अगर आप वाम पक्ष की तरफ है तो इस हस्तक्षेप को ‘त्रासदी’ कहेंगे. वहीं अगर आप अपने दक्षिणपंथी रुझान को साबित करना चाहते हैं तो आप इसे कहेंगे कि ‘पश्चिमी लोकतंत्रों ने इराक़़ को आज़ाद’ कराया.
पहले समूह वाले लोगों के लिए इराक़ में क़यामत के दिन तक जो भी ग़लत होगा, उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ सद्दाम को सत्ता से हटाना माना जाएगा. 2003 का युद्ध ईसाइयों की ‘मूल पाप’ वाली अवधारणा का राजनीतिक संस्करण है.
वहीं दूसरे समूह के लोगों के लिए इराक़ी लोग जो भी उपलब्धि हासिल करेंगे, वे उन्हें 'पश्चिमी लोकतंत्र की विजय' के तौर पर पेश करेंगे.
विदेशों में पश्चिमी प्रभाव की जब भी बात होती है तो इन्हीं दो विचारधाराओं की प्रतिध्वनियां सुनने को मिलती हैं- अपराधबोध और घमंड.
सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया जाना इराक़ के हालिया इतिहास की एक बड़ी घटना है. इसके बाद से इराक़ियों के खाते में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी भी. दोनों ही मामलों में युद्ध ने कहीं न कहीं उन्हें संभावनाएं मुहैया कराईं. दोनों ही मामलों में श्रेय और आलोचना इराक़ियों के खाते में जाएगी.
इराक़ में जो कुछ हो रहा है, वो सांप्रदायिक युद्ध नहीं है बल्कि संप्रदायवादियों का युद्ध है जिसका इतिहास 15 सदी पुराना है, उससे भी बहुत पहले जब नक्शे पर अमरीका और ब्रिटेन जैसे नए देश प्रकट हुए थे.
पश्चिमी जगत के वामपंथियों और दक्षिणपंथियों को इराक़ के मुद्दे पर ख़ूब घरेलू राजनीति करने दी जाए. इस बारे में सौम्य विश्लेषण के लिए एक स्पष्ट अवधारणा की ज़रूरत है. बहुत सारी व्याख्याएं और विवरण आखिरकार भ्रम ही पैदा करते हैं.
इराक़ी लोग: आक्रमण, हालात और खुद अपनी ही गलतियों के शिकार
एलिना सुपोनीना
अंतरराष्ट्रीय मामलों की रुसी जानकार और राजनीति शास्त्री
इराक़ में चरमपंथियों का आना और कई शहरों पर क़ब्ज़ा करना दिखाता है कि वहां सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है.
पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक़ में लोकतंत्र कायम करना चाहते थे. इसकी बजाय इराक़ अब ध्वस्त होने के कगार पर है. दहशत वहां आम हो गई है.
धार्मिक समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी को 2006 से अमरीका का समर्थन हासिल है, वह भी अब एक तानाशाह में तब्दील हो गए हैं.
इराक़ में हिंसा बढ़ने के बाद मेरी बातचीत निनेवेह प्रांत के गवर्नर अतहील अल-नुजैफी से हुई थी. निनेवेह प्रांत की राजधानी मोसूल वो पहला शहर था जिस पर आईएसआईएस के चरमपंथियों ने क़ब्ज़ा किया.
गवर्नर वहां से भाग गए. मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा. अतहील अल-नुजैफी का मानना है कि प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी की नीतियों के चलते कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला है.
सुन्नी बहुल इलाकों में स्थानीय अधिकारियों के लिए दिन ब दिन स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा है. जिहादियों ने माहौल को भांप लिया और इन इलाकों पर आसानी से क़ब्ज़ा कर लिया. कई इलाकों में तो उनका स्वागत भी हुआ.
अमरीका के लिए मौजूदा हालात एक बड़ी विफलता है क्योंकि उसके सैनिक 2003 से 2011 तक इराक़़ में रहे. उनकी रणनीति गलत साबित हुई. उनके हमले के लक्ष्य पूरे नहीं हुए. लेकिन मैं उन कुछ रूसी राजनीतिक पंडितों से कतई सहमत नहीं हूं जो मानते हैं कि अमरीका का इरादा मध्य पूर्व में अव्यवस्था फैलाना था.
मेरी राय में, अभी इराक़ में मौजूदा स्थिति पर किसी का नियंत्रण नहीं है. और ये नाकामी अमरीका की प्रतिष्ठा के लिए एक धक्का है.
फिर भी, दो साल से इराक़ी अच्छी ख़ासी आज़ादी महसूस कर रहे थे. विदेशी सैनिक चले गए. भारी मात्रा में गैस और तेल है. अब हर चीज के लिए अमरीकियों को जिम्मेदार ठहराना बंद होना चाहिए.
अपने देश के लिए इराक़ी ही जिम्मेदार हैं. और हमें ख़ुद को इस बात का भरोसा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है कि इराक़ियों पर कोई तानाशाह ही राज कर सकता है. इराक़ियों को अपने खुद के लोकतंत्र की ज़रूरत है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)